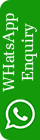भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका: प्रमुख न्यायिक वादों का विश्लेषण
Author(s): ललित काण्डपाल
Abstract: संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, हालांकि 1956 के सातवें संशोधन ने दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया। राज्यपाल का पद एक गरिमामय संवैधानिक पद है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ही दल का प्रभुत्व रहने के कारण राज्यपाल की भूमिका कम महत्वपूर्ण थी। हालांकि, 1967 के बाद जब कई राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें बनीं, तो राज्यपालों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का अधिक प्रयोग करना पड़ा, जिससे उनकी भूमिका अधिक प्रमुख हो गई।
कुछ राज्यपालों पर निष्पक्षता की कमी का आरोप लगा है, खासकर जब उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की या राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोका। राज्यपालों को अक्सर उनके कार्यकाल से पहले हटाए जाने या स्थानांतरित किए जाने से इस पद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सरोजिनी नायडू ने इस पद को "सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया" कहा था, जो इसकी सीमित शक्तियों को दर्शाता है। यह भी आलोचना की जाती है कि केंद्र सरकार इस पद का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करती है।
DOI: 10.33545/26646021.2025.v7.i8b.625Pages: 86-91 | Views: 300 | Downloads: 62Download Full Article: Click Here

How to cite this article:
ललित काण्डपाल.
भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका: प्रमुख न्यायिक वादों का विश्लेषण. Int J Political Sci Governance 2025;7(8):86-91. DOI:
10.33545/26646021.2025.v7.i8b.625