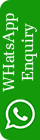कà¥à¤®à¤¾à¤° सौरà¤, नेहा गà¥à¤ªà¥à¤¤à¤¾.
à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ लोकतनà¥à¤¤à¥à¤° à¤à¤µà¤‚ जातिवादी राजनीति. Int J Political Sci Governance 2019;1(2):17-20. DOI:
10.33545/26646021.2019.v1.i2a.15